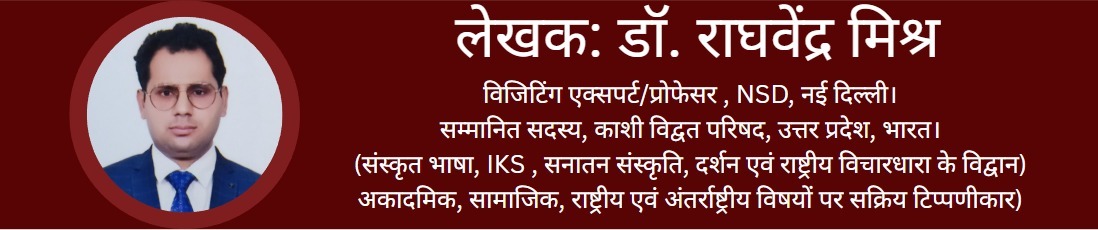उपनिषद केवल दार्शनिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव चेतना की गहन खोज के जीवन्त अभिलेख हैं। इनमें वर्णित तीन बाल पात्र– नचिकेता, सत्यकाम जाबाल और श्वेतकेतु – अपनी जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और आत्म-खोज की यात्रा से हमें प्रेरित करते हैं।
उनकी चेतना न केवल प्राचीन भारत के शैक्षिक, सामाजिक और आध्यात्मिक परिवेश को उजागर करती है, बल्कि आज के युग में भी सत्य और आत्म-विज्ञान की अनुसन्धान को प्रासंगिक बनाती है क्योंकि वर्तमानकालिक पञ्चतन्त्र के ’कीलोत्पाटीव वानर’तथाकथित २१वीं शताब्दी की मनुष्यता/मानवता बौद्धिक-द्वन्द्व,कार्मिक-द्वन्द्व,भावनात्मक द्वन्द्व के साथ साथ भाषाई अतिचार से पीडित है ।
हिंसा और भय पर आश्रित उन्नति, विकास के नारे वाली मानवता को अब ढोंग एवम् पाखण्ड के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए इन औपनिषदिक बालक-त्रय की शरण में उपस्थित होना चाहिए ताकि निकट भविष्य में यह अर्ध मृत-प्राय पृथिवी अपनी सम्पदा सहित पुनर्जीवित हो सके।
इसी कारण इन बालक-त्रय की चेतना के आयामों का परिभाषिकीकरण करना आवश्यक है ताकि मनुष्यता अपनी बौद्धिक, भावनातमक एवम् कार्मिक विकृतियों एवम् विसंगतियों को समझ कर सरल, निर्मल, निश्छल, पारदर्शी व्यवहार की अग्रसर हों ताकि भविष्य में मनुष्यता अपने अस्तित्व और अस्मिता के प्रति आश्वस्ति के भाव सफल, सार्थक जीवन जी सके ।
नचिकेता : मृत्यु के पार सत्य का साहसी अन्वेषक
कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता अपनी निर्भीक जिज्ञासा से यमराज के समक्ष मृत्यु और आत्मा के रहस्यों की खोज करते हैं। उनकी चेतना हमें सिखाती है कि सत्य की खोज किसी भी भय या सीमा से परे है।
सत्यकाम जाबाल : सत्यनिष्ठा का जीवंत प्रतीक
छान्दोग्य उपनिषद के सत्यकाम जाबाल अपनी सामाजिक अस्पष्टता के होने पर भी सत्य कथन की क्षमता और योग्यता के बल पर गुरु हरिद्रुम गौतम के शिष्य बनते हैं। उनकी चेतना सत्य के प्रति अडिग श्रद्धा और नैतिक उत्कृष्टता को दर्शाती है।
श्वेतकेतु : आत्म-ज्ञान की विनम्र यात्रा
श्वेतकेतु छान्दोग्य उपनिषद के एक जिज्ञासु बालक, अपने पिता उद्दालक के मार्गदर्शन में अहंकार से विनम्रता और बाह्य ज्ञान से आत्म-विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। उनकी चेतना आत्म-खोज की सहज किंतु गहन यात्रा का प्रतीक है।
इसमें जानने एवम् समझने योग्य विषय:
१. चेतना का समवाय : तीनों बालकों की जिज्ञासा, सत्य कथन की क्षमता और आत्म-विज्ञान के बीच समानताएँ और विशिष्टताएँ।
२. आधुनिक प्रासंगिकता : सामाजिक गतिशीलता, मनोवैज्ञानिक प्रेरणा, सांस्कृतिक मूल्य, दर्शनशास्त्रीय प्रश्न और शैक्षिक दृष्टिकोणों के माध्यम से इन कथाओं का विश्लेषण।
३. प्रेरणा और प्रासंगिकता : औपनिषदिक मूल्यों को आज के जीवन में कैसे अनुप्रयुक्त (लागू) करें, और कैसे ये कथाएँ हमें सत्य, नैतिकता और आत्म-जागरूकता की ओर ले जाती हैं।
तो यदि आप ढोंगी, पाखण्डी और रूग्ण आत्महन्ता बुद्धिजीवी, सिकुलर, वामपन्थी नहीं हैं और मनुष्यता और अर्ध-जीवित पृथिवी के लिए उभरते हुए खतरों के प्रति सजगता सहित आप दर्शन, उपनिषद और भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि रखने वाले जिज्ञासु हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और शोधकर्ता हैं जो प्राचीन ज्ञान को समकालीन संदर्भों से जोड़ना चाहते हैं या वे सभी जो आत्मानुसन्धान और सत्य-कथन क्षमता की गहन यात्रा में रुचि रखते हैं, तो आप सादर आमन्त्रित हैं।
इन बाल-त्रय - नचिकेता, सत्यकाम और श्वेतकेतु से प्रश्न और जिज्ञासा के अन्तर को, सत्य की कथन की क्षमता की खोज को और आत्मानुसन्धान के व्यवहार एवम् स्तर को सीखने और समझने का प्रयास करें। यह एक अवसर है वैदिक दर्शन एवम् दृष्टि को गहनता से समझने और उसे अपने जीवन में उतारने का। नचिकेता, सत्यकाम जाबाल और श्वेतकेतु की चेतना हमें निर्देशित करती है कि सत्य और आत्म-विज्ञान की खोज आयु, परिस्थिति या सामाजिक बंधनों से परे है।
उपनिषद केवल दार्शनिक ग्रंथ नहीं
उपनिषद केवल दार्शनिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय मानस की उच्चतम जिज्ञासाओं, मूल्यबोध और आत्मिक उन्नयन की यात्रा के अभिलेख हैं। इस वैचारिक यात्रा में कुछ बाल पात्र ऐसे हैं, जिन्होंने ज्ञान, सत्य और आत्मानुसन्धान की दिशा में जो दृष्टिकोण अपनाया, वह आज भी हमारी शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को प्रेरणा देता है। नचिकेता, सत्यकाम जाबाल और श्वेतकेतु– ये तीन बालक उपनिषदों के ऐसे अद्भुत पात्र हैं जिनकी चेतना किसी आयु की सीमा में नहीं बंधती। यह सम्वादशाला में उन तीनों के वैचारिक स्वरूप का समकालीन संदर्भों में विवेचन का प्रयास है।
नचिकेता– मृत्यु के पार जाकर सत्य की खोज
सहोवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति।
द्वितीयं तृतीयं तँ होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥ कठोपनिषद् 1.1.4
तब नचिकेता ने अपने पिता से पूछा — "पिताजी! आप मुझे किसे देंगे?" पिता ने उत्तर दिया — "मैं तुम्हें मृत्यु (यमराज) को अर्पित करता हूँ।"
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद् वीतमन्युर्गौतमो माऽभि मृत्यो ।
त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत्प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥ कठोपनिषद् 1.1.10
हे मृत्यु! गौतम (नचिकेता के पिता) का चित्त शांत हो जाए, वह प्रसन्न मन वाला हो और क्रोध से रहित हो जाए। तुम मुझे अपने आशीर्वाद से भेजो, ताकि वह मुझे पहचानकर स्नेहपूर्वक बोले। यही मेरा पहला वर है, जिसे मैं माँगता हूँ।
स त्वमग्निँ स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वँ श्रद्दधानाय मह्यम् ।
र्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण ॥ कठोपनिषद् 1.1.13
हे मृत्यु! तुम उस अग्निविद्या को जानते हो जो स्वर्ग की प्राप्ति कराती है- कृपया वह मुझे बताओ, क्योंकि मैं श्रद्धापूर्वक उसे जानना चाहता हूँ। स्वर्ग लोक में रहने वाले अमरता का अनुभव करते हैं। यह मेरा दूसरा वर है।
येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येस्तीत्येके नायमस्तीति चैके ।
एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाऽहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ कठोपनिषद् 1.1.20
जब कोई मनुष्य मरता है तो इस विषय में संदेह रहता है, कुछ कहते हैं कि वह (आत्मा) रहता है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहता। इस विषय को जानने की शिक्षा मैं आपसे चाहता हूँ। यही मेरा तीसरा वर है।
कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता, एक ऐसे बालक हैं जो अपने पिता के यज्ञ-कर्म में मानवीय आत्म-प्रवञ्चना और प्रमाद से असंतुष्ट होकर प्रश्न करते हैं– "मैं किसे अर्पित किया जाऊँगा?"। यमलोक की यात्रा, यमराज से संवाद, और 'नाचिकेतस् अग्नि' का ज्ञान प्राप्त कर वह आत्मा और ब्रह्म के गहन रहस्यों तक पहुँचते हैं।
नचिकेता की चेतना– जिज्ञासा, निडरता और आत्म-तत्त्व की खोज से ओतप्रोत है। वह उस यथार्थ को जानना चाहता है जो मृत्यु के पार है, अतीत है।
सत्यकाम जाबाल – सामाजिक बंधनों से परे सत्य की प्रतिष्ठा
सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्रयांचक्रे ब्रह्मचर्यं भवति
विवत्स्यामि किंगोत्रो न्वहमस्मीति ॥ छान्दोग्य उपनिषद् 4.4.1
(सत्यकाम जाबाल नामक बालक ने अपनी माता जबाला से पूछा- “मां! मैं ब्रह्मचर्य (विद्या) की प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाना चाहता हूँ। कृपया बताओ कि मेरा गोत्र क्या है?”
स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विंशतिवर्षः सर्वान्वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय तꣳह पितोवाच ॥ छान्दोग्य उपनिषद् 6.1.2)
छान्दोग्य उपनिषद में वर्णित सत्यकाम का जीवन हमें बताता है कि औपनिषदिक भारत में जन्म से अधिक महत्त्व ‘सत्य’ और ‘योग्यता’ को दिया गया। जब वह अपने पिता का नाम नहीं बता पाता, तब भी गुरु हरिद्रुम गौतम उसे केवल उसकी सत्यनिष्ठा के आधार पर शिष्य बनाते हैं। सत्यकाम की चेतना– नैतिक प्रमाणिकता, सत्य के प्रति अडिग श्रद्धा और आंतरिक उत्कंठा का जीवंत उदाहरण है। वह स्वयं प्रकाशमान सत्य के पथ का अनुगामी है।
श्वेतकेतु – आत्म-ज्ञान की सहज किन्तु जटिल यात्रा
श्वेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना अनूचानमानी स्तब्धोस्युत तमादेशमप्राक्ष्यः येनाश्रुत श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति ॥ छान्दोग्य उपनिषद् 6.1.3
(जब वह बारह वर्ष की आयु में गुरुकुल गया और चौबीस वर्ष की आयु तक सभी वेदों का अध्ययन कर लिया,तब वह महान बुद्धि वाला, अपने ज्ञान पर गर्व करता हुआ, आत्ममुग्ध होकर लौटा। तभी उसके पिता ने उससे कहा... "हे श्वेतकेतु, हे प्रिय पुत्र! तुम महान बुद्धि वाले, शास्त्रों में पारंगत और आत्मगर्वी बनकर लौटे हो, पर क्या तुम उस उपदेश (आत्मविद्या) को जान पाए हो - जिसे जान लेने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है? जिससे अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है, अश्रुत भी श्रुत हो जाता है? हे भगवन् (पुत्र), वह उपदेश कैसा होता है?")
श्वेतकेतु छान्दोग्य उपनिषद के एक ऐसे पात्र हैं जो प्रारम्भ में ज्ञान के अभिमान से ग्रस्त हैं, किन्तु जब पिता उद्दालक उन्हें आत्मा और ब्रह्म के सूक्ष्म ज्ञान की ओर ले जाते हैं– तब वह अहंकार से विनम्रता की ओर, और बाह्य ज्ञान से आत्म-ज्ञान की ओर प्रवृत्त होते हैं। श्वेतकेतु की चेतना– एक ऐसी चेतना है जो अपने अधूरेपन को पहचानती है और उसकी पूर्ति आत्म-विज्ञान में खोजती है।
बालक-त्रय की समवेत चेतना के आयाम :-
1. ज्ञान के प्रति उत्कंठा: तीनों पात्रों में बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जिज्ञासा प्रमुख है।
2. सामाजिक संरचनाओं की चुनौती : वे परंपराओं, सामाजिक सीमाओं, और व्यक्तिगत भ्रमों को चुनौती देते हैं।
3. आत्मा की खोज: तीनों की चेतना आत्म-विज्ञान की ओर उन्मुख है – यह उपनिषदों की मूल प्रवृत्ति भी है।
आधुनिक सन्दर्भों में तीनों पात्रों की चेतना का बहु-आयामी विश्लेषण :-
1. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण :-
क) सामाजिक गतिशीलता : सत्यकाम का उदाहरण बताता है कि योग्यता, नैतिकता और सत्यनिष्ठा सामाजिक पहचान से ऊपर हैं।
ख) पारिवारिक सम्बन्ध : नचिकेता और श्वेतकेतु अपने-अपने पिता से ज्ञान के माध्यम से सम्बन्ध विकसित करते हैं। सत्यकाम अपनी माँ के साथ पवित्र संवाद के माध्यम से आत्मगौरव अर्जित करते हैं।
2. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण :
क) स्व-प्रेरणा : तीनों पात्र आत्म-प्रेरित हैं। वे किसी भय या लोभ से नहीं, बल्कि सत्य की लालसा से प्रेरित हैं।
ख) आत्म-संवाद: उनका चेतन पथ आन्तरिक संघर्षों और आत्म-प्रश्नों से गुजरता है, जिससे आत्मिक परिपक्वता आती है।
3. सांस्कृतिक दृष्टिकोण :
क) गुरु-शिष्य परंपरा: इन पात्रों की कहानियाँ वैदिक गुरु-शिष्य संबंधों की गरिमा को दर्शाती हैं।
ख) मूल्यबोध : नैत्कता, श्रद्धा, सत्यनिष्ठा, और निडरता– ये औपनिषदिक मूल्य इन पात्रों की चेतना में साकार होते हैं।
4. दर्शन-शास्त्रीय दृष्टिकोण :
क) अस्तित्ववादी प्रश्न: नचिकेता का संवाद जीवन, मृत्यु और आत्मा के अस्तित्व को स्पर्श करता है।
ख) आधिभौतिकी और ज्ञानमीमांसा: श्वेतकेतु और सत्यकाम की यात्रा ज्ञान के साधन, उसकी उपपत्ति और सीमाओं की पड़ताल करती है।
5. शैक्षिक दृष्टिकोण :
क) शिक्षा का लक्ष्य: इन पात्रों की चेतना समग्र शिक्षा की अवधारणा को दर्शाती है – जहाँ बौद्धिक, नैतिक और आत्मिक विकास समान रूप से आवश्यक हैं।
ख) शिक्षण पद्धति: संवाद, प्रश्नोत्तर, प्रतीकों के माध्यम से शिक्षा का वैदिक ढाँचा स्पष्ट होता है।
अतः यह कहना सम्भव है कि नचिकेता, सत्यकाम और श्वेतकेतु की चेतना उपनिषदों की अंतर्यात्रा का त्रैविध रूप हैं – प्रश्न, सत्य और आत्म की खोज। यह चेतना न तो केवल धार्मिक है, न दार्शनिक भर, यह एक जीवित शिक्षा है– जो आज के संदर्भों में भी प्रासंगिक है। इन बालकों की जीवनगाथाएँ हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी प्रश्न करें, सत्य की खोज करें, और आत्मा के स्वरूप को जानें और समझें।